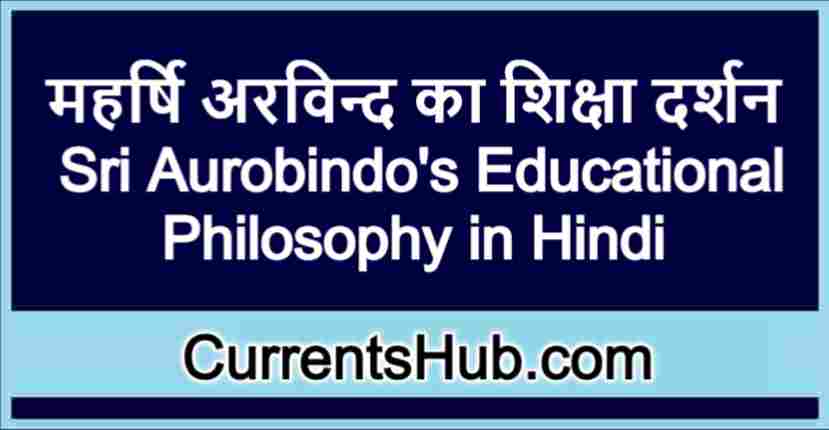
अनुक्रम (Contents)
महर्षि अरविन्द का शिक्षा दर्शन (Sri Aurobindo’s Educational Philosophy)
श्री अरविन्द की यह धारणा थी कि जीव की आत्मा से ज्ञान सदा सुषुप्तावस्था में गुप्त रहता है। शिक्षा का आधार या वाहन अथवा यन्त्र अन्त:करण है, अतः अन्तःकरण की संरचना पर उन्होंने गम्भीर विचार किया है। उनके अनुसार अन्तःकरण के चार पटल होते हैं प्रथम पटल है चित्त जो अन्य तीन पटलों का आधार है। जब हम कोई बात याद करते हैं तो वह छनकर चित्त में एकत्र होती है। यह भूतकालिक मानसिक संस्कार है। चित्त रूपी स्मृति-कोषों से ही क्रियाशील स्मृति कभी-कभी कुछ चीजों को चुन लेती है। यह चुनाव उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त हो सकता है, अतः इसके प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
अन्त:करण का दूसरा पटल ‘मानस’ है। इसमें अन्य पटल एकत्र होते हैं और इसे ही दर्शन की भाषा में मस्तिष्क कहा जाता है। इसका कार्य ज्ञानेन्द्रियों से प्रत्ययों को ग्रहण करना और उसे विचारों में परिणत करना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध सम्बन्धी सूचना ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त होती है। इन सूचनाओं को विचारों में परिवर्तित कर देना मस्तिष्क का काम है । मस्तिष्क स्वयं भी प्रत्ययों एवं प्रतिमाओं को ग्रहण कर लेता है । इस प्रकार पाँच ज्ञानेन्द्रियों के अतिरिक्त यह स्वयं भी एक उपकरण है। उत्तम विचार के लिए पाँचों ज्ञानेन्द्रियों एवं मस्तिष्क का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। इन छहों उपकरणों को सक्षम बनाना है।
अन्तःकरण का तीसरा पटल बुद्धि है। मस्तिष्क जिस ज्ञान को प्राप्त करता है, उसे व्यवस्थित करने का वास्तविक यन्त्र बुद्धि है। यह विचार शक्ति का पटल है। शिक्षक के लिए बुद्धि का सर्वाधिक महत्त्व है। इसमें रचनात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक शक्तियाँ निहित होती हैं। बुद्धि दो भागों में विभक्त है। इसका प्रथम पक्ष या दाहिना हाथ सोचने, विचारने, निर्णय करने, स्मरण करने, आदेश देने, अवलोकन करने एवं परिकल्पना करने की शक्तियों से सम्पन्न होता है और दूसरा पक्ष या बायाँ हाथ आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शक्तियों से युक्त होता है। बुद्धि का दूसरा पक्ष अन्तर बताने, अन्वेषण करने एवं तर्क-वितर्क के बाद परिणाम निकालने में कुशल होता है। दायाँ भाग ज्ञान का अधिष्ठाता है, बायाँ भाग ज्ञान का सेवक मात्र है। इन शक्यिों से तर्कपूर्ण विचार सम्भव है, अतः बुद्धि के दोनों भावों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है।
अन्त:करण का चतुर्थ पटल सत्य के अन्तर्दृष्टिपरक प्रत्यक्षीकरण की शक्ति है। इससे ज्ञान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है और इसके आधार पर व्यक्ति भविष्य का कथन करने में समर्थ होता है। मस्तिष्क की यह शक्ति अभी पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकी। यह विकास की अवस्था में है। किन्तु मानव के अन्तःकरण में यह शक्ति है अवश्य और यदि इस दुर्लभ शक्ति का विकास किया जाय तो मानवता की समस्याओं का समाधान मिल जायेगा। मानव की तार्किक बुद्धि अपनी चंचलता एवं पक्षपातपूर्णता के कारण इस शक्ति को विकृत कर देती है। इस शक्ति के विकास में अभी तक बहुत कम ध्यान दिया गया है अतः शिक्षकों को इस ओर ध्यान देना आवश्यक है।
शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Education)— श्री अरविन्द के अनुसार वास्तविक, जीवन्त एवं सच्ची शिक्षा वह है जो बालक की सुषुप्त शक्तियों को उबुद्ध करे । व्यष्टि एवं समष्टि की संकीर्ण सीमा से निकाल कर बालक को मानवतावादी एवं समग्रवादी बनाना है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य ने आत्मा, मस्तिष्क एवं विवेक की शक्तियों तथा ‘स्व’ का विकास कर लिया है। शिक्षा को मानव आत्मा की माँगों की पूर्ति करनी चाहिए।
शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति की सर्वोत्तम शक्ति को विकसित करना होना चाहिए। श्री अरविन्द ने ‘ऐसेज ऑन द गीता’ भाग-2 में लिखा है, “बालक की शिक्षा को उसकी प्रकृति में जो कुछ सर्वोत्तम, सर्वाधिक अन्तरंग और जीवनपूर्ण है, उसको व्यक्त करना होना चाहिए, मनुष्य की क्रिया और विकास जिस साँचे में ढलने चाहिए, वह उसके अन्तरंग गुण और शक्ति का साँचा है। उसे नयी वस्तुएँ अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। परन्तु वह उनको सर्वोत्तम रूप से और सबसे अधिक प्राणमय रूप में स्वयं अपने विकास, प्रकार और अन्तरंग शक्ति के आधार पर प्राप्त होगा ।”
अतः आत्म-शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्र करना शिक्षा नहीं है शिक्षा का काम मानव के मस्तिष्क एवं शक्तियों का सृजन करना है। सामान्य मस्तिष्क के अतिरिक्त एक विशिष्ट मस्तिष्क भी होता है जो जीवन एवं विषयों के परे स्थित है और जो इस संसार में अपना प्रकाशन करता है। इस विशिष्ट मस्तिष्क की अनुभूति करना – कराना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए।
राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है मानव आत्मा एवं सार्वभौमिक आत्मा के मध्य की कड़ी है। इस दृष्टि से श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीयता के अच्छे उपासक होते हुए भी राष्ट्रवाद के समर्थक हैं और शिक्षा को राष्ट्रीयता पर आधारित करना चाहते हैं। वे कहते हैं, “हम जिस शिक्षा की खोज में हैं, वह एक भारतीय आत्मा और आवश्यकता तथा स्वभाव और संस्कृति के उपयुक्त शिक्षा है, केवल ऐसी शिक्षा नहीं है जो भूतकाल के प्रति भी आस्था रखती हो, बल्कि भारत भी विकासमान आत्मा के प्रति, उसकी भावी आवश्यकताओं के प्रति, उसकी आत्मोत्पत्ति की महानता के प्रति, और उसकी शाश्वत आत्मा के प्रति आस्था रखती है।
श्री अरविन्द के शिक्षा सम्बन्धी आदर्शों से दूसरे शिक्षाशास्त्री भी सहमत हैं और उनके बहुत से नये-नये प्रयोग अब शिक्षा के अंग बन चुके हैं। पर उनकी विशेष देन इस बात में है कि उन्होंने व्यक्तित्व के सामंजस्य, सन्तुलन और सर्वांगीण विकास पर बल दिया। उनको धारणा थी कि शिक्षा सौंदर्य पर आधारित होनी चाहिये। तभी मनुष्य को सत्य की उपलब्धि हो सकती है। इस प्रकार सत्य, शिव और सुन्दर को उन्होंने अपने शिक्षा सम्बन्धी आदर्श में एक रूप में समन्वित कर लिया था।
पाठ्यक्रम (Curriculum)- श्री अरविन्द ने जो शिक्षा के उद्देश्य बताये, उन्हें प्राप्त करने हेतु उन्होंने विस्तृत पाठ्यक्रम की रचना की जिसकी उपयोगिता सर्वविदित है।
शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिये, इस बात पर वे बराबर बल देते रहे। इसका कारण उनकी यह मान्यता थी कि शिक्षा सबसे अधिक प्रभावपूर्ण तब होती है, जब उसे अज्ञात रूप से आत्मसात् किया जाता है। कोई विदेशी भाषा चाहें कितनी ही समृद्ध क्यों न हो, *उसके अपने अलग संदर्भ होते हैं, अलग वातावरण होता है, चूँकि बच्चा उन संदर्भों और वातावरण से परिचित नहीं होता, इसलिये वे उसके मन पर भार स्वरूप हो जाते हैं। जब बच्चा कोई बात विदेशी भाषा में सुनता है, तब उसका मन विषय और भाषा के बीच में बँट जाता है, जबकि मातृभाषा में सिखायी गयी कोई भी बात इस तरह ध्यान को नहीं बाँटती।
महर्षि अरविन्द ने मातृभाषा के साथ-साथ यह भी कहा कि विश्व अब एकत्व की ओर बढ़ रहा है, अतः किसी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा से परहेज नहीं होना चाहिए।
इस प्रकार महर्षि अरविन्द ने विदेशी भाषा के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा को संकुचित, औपचारिक एवं असाहित्यिक बताकर उसका विरोध किया और शिक्षा को भारतीय दर्शन, आदर्श, कला, साहित्य एवं संस्कृति पर आधारित किया पर वे किसी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के ज्ञान को भी महत्त्वपूर्ण मानते थे।
महर्षि अरविन्द ने अपने पाठ्यक्रम में अनेक विषयों के साथ-साथ क्रियाओं और पाठ्यान्तर क्रियाओं को विशेष महत्त्व दिया। आधुनिक समय में, पाठ्यक्रम में, इन क्रियाओं के महत्त्व को स्वीकार किया गया है।
श्री अरविन्द द्वारा समर्थित पाठ्यक्रम अत्यन्त विस्तृत है। सबसे पहले बालक को उसके चारों ओर के परिवेश से परिचित कराना चाहिए। बालक की मानसिक शक्तियों के लिए पाठ्य विषयों की योजना होनी चाहिए। काव्य, कला और संगीत की शिक्षा आवश्यक है। काव्य व्यक्ति के संवेगों का उन्नयन करता है। कला संवेगों में सन्तुलन स्थापित करती हैं। और संगीत संवेगों की गहराई में व्यक्ति को ले जाता है। अतः इनका शिक्षण आवश्यक है। इसमें सृजनात्मकता तथा कल्पनाशीलता का विकास होता है।
शिक्षण-विधि (Method of Teaching)- आजकल इस बात पर बल दिया जाता है कि छात्रों को कक्षा में सक्रिय बनाया जाए। श्री अरविन्द सक्रियता के समर्थक तो हैं, किन्न वे केवल सक्रियता के पक्षपाती नहीं हैं। उनका विचार है कि बालक को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए कि वे निष्क्रियता से भी सीख सकें, मस्तिष्क को निष्क्रिय करने का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। छात्रों को इस बात का अभ्यास होना चाहिए कि वे आवश्यकता पड़ने पर मस्तिष्क को निष्क्रिय बना दें।
शिक्षण में छात्र की इच्छा का अत्यधिक महत्त्व है । महत्त्व की बात यह नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, वरन् यह कि छात्र किस विषय में पढ़ने की रुचि रख रहा है । अत: छात्र की रुचि के आधार पर हमें अपनी शिक्षण विधि को नियोजित करना चाहिए। जब हम कोई विषय पढ़ाने चलते हैं तो पहले उस विषय में छात्र की रुचि उत्पन्न करनी है। पहले से नहीं भी है तो पढ़ाते समय शिक्षण-शैली ऐसी हो कि छात्र पाठ्य-विषय में रुचि लेने लगे।
विज्ञान शिक्षण में छात्र की जिज्ञासा प्रवृत्ति को उबुद्ध करना आवश्यक है। प्राकृतिक पदार्थों के निरीक्षण को प्रोत्साहित करना है। फूलों के निरीक्षण एवं तुलना के द्वारा छात्र-विज्ञान को सीखें भूमि और पाषाणों के निरीक्षण द्वारा भूगर्भशास्त्र को सीखें, पशुओं के सूक्ष्म निरीक्षण से जीव-विज्ञान सीखें। इस प्रकार आस-पास के वातावरण को आधार बनाकर विज्ञान की शिक्षा दी जाए। खगोल विद्या सीखने के लिए तारों का निरीक्षण आवश्यक है।
छात्रों की जिज्ञासा और बौद्धिक चेतना को दर्शन पढ़ने में उबुद्ध करना है । इतिहास पढ़ाते समय मानवता की कहानी इस प्रकार कहनी है कि छात्रों में देशभक्ति और पूजा की भावना जाग्रत हो। इन भावनाओं को आधार बनाकर यदि इतिहास पढ़ाया जाता है तो वह मनोरंजक भी होगा।
श्री अरविन्द का मत है कि बालक की शिक्षा वर्णमाला से नहीं प्रारम्भ होनी चाहिए। सबसे पहले उसे प्रकृति का निरीक्षण करना चाहिए। पुष्पों, लताओं, सितारों, पशु-पक्षियों, वनस्पतियों आदि का निरीक्षण करना पहले आवश्यक है। यह एक प्रकार से वस्तुओं पर प्रयोग है। इसके बाद शब्दों का ज्ञान देना है। शब्दों के प्रयोग का छात्रों को अधिक अभ्यास कराना चाहिए। बालक पहले शब्द का रूप, स्वर और अर्थ का सम्यक बोध करे और तत्पश्चात् विभिन्न शब्दों की समानताएँ एवं असमानताएँ समझें। इससे उसे व्याकरण बहुत सीखने में मदद मिलेगी। शब्द प्रयोग के द्वारा उसमें साहित्यिक योग्यता का विकास होगा।
शिक्षण-विधि ऐसी हो कि छात्र अनेकानेक सूचनाएँ प्राप्त करने को अध्ययन का साक्ष्य न मानें। वह सामग्री को याद करने को महत्त्वपूर्ण न मानकर ज्ञान प्राप्त करने के कौशलों के विकास को मूल्यवान समझें। इस प्रकार छात्र में स्मृति, निर्णय, कल्पना, तर्क-वितर्क, प्रत्यक्षण, चिन्तन जैसी शक्तियों का विकास करना है, न कि केवल विषय-सामग्री को याद करना। अतः शिक्षण-विधि ऐसी हो कि विषय सामग्री का चयन कुशलतापूर्वक होता चाले।
श्री अरविन्द के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। मातृभाषा के ही माध्यम से राष्ट्र का स्वरूप बालक के समक्ष उपस्थित होता है। अपने देश के साहित्य और इतिहास को समझने का सबसे अच्छा माध्यम मातृभाषा ही है। अपने चारों ओर के परिवेश का ज्ञान मातृभाषा को छोड़कर और किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है ? जब छात्र मातृभाषा पर अधिकार कर ले तो उसे अन्य विशेष भाषाएँ सिखानी चाहिए।
व्यावहारिक शिक्षा के साथ-साथ श्री अरविन्द ने धार्मिक शिक्षा को, शिक्षा के साथ देना आवश्यक समझा। उनके अनुसार “धर्म वह आत्म-शक्ति है जो आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करती है। इस संसार में जब व्यक्ति आत्मान्वेषण करते हुये अमरता का आनन्द प्राप्त करता है अर्थात् अपने श्रेष्ठ स्वरूप की सम्भावनाओं के अन्वेषण के लिये वह मित्रता, सहानुभूति और शान्ति का अभिवर्धन करता है तब कहीं जाकर अन्तरात्मा बाहरी क्रिया-कलापों को नियमित एवं रूपायित करती है और इसके प्रत्येक अंग में मनुष्य ईश्वरीय प्रयोजन की अभिव्यक्ति देखता है और ईश्वर शब्द का ठीक तथा पूरा आशय समझता है।”
महर्षि अरविन्द औपचारिक रूप से पाठों में विभाजित धार्मिक शिक्षा में विश्वास नहीं करते। धर्म कोई विभाजित वस्तु नहीं है जिसे विद्यालय में पाये जाने वाले पाठ्यक्रम में अन्य विषयों के अनुसार साप्ताहिक अथवा दैनिक समयान्तरों में विभक्त किया जा सके। धार्मिक शिक्षा को हम वाल्यकाल से ही ऐसे वातावरण में रहकर प्राप्त करते हैं जहाँ कि आध्यात्मिक संसार के सत्य को कृत्रिम महत्त्व की आवश्यकताओं की भीड़ से धुंधला न कर दिया जाये। जहाँ पर अवकाश से परिपूर्ण खुली जगह एवं शुद्ध वायु से परिपूर्ण शांत प्रकृति में सदा जीवन हो और जहाँ पर मनुष्य अपने सम्मुख उपस्थित सतत् जीवन पूर्ण आस्था से जी सके।
इन्द्रियों का प्रशिक्षण (Training of Sense Organs)- श्री अरविन्द के अनुसार बालक की शिक्षा का प्रारम्भ आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के प्रशिक्षण से होना चाहिए । अनुभव की यथार्थता का आधार यही प्रशिक्षण है। यदि इन इन्द्रियों में कोई शारीरिक विकृति है तो उसका तत्काल उपचार कराना चाहिए। ज्ञानेन्द्रियों में यदि कोई अपूर्णता है। तो उस अपूर्णता के कारण को समझना चाहिए। ज्ञानेन्द्रियों को सबल बनाना है। इन्हें सचेष्ट एवं सशक्त बनाने के लिए नाड़ियों का सशक्त होना आवश्यक है। ज्ञान-तन्तुओं के कार्य में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि नाड़ियों के कार्य में कोई ऐसी बाधा है जिसे वैद्य दूर नहीं कर सकते तो उन बाधाओं को ‘नाड़ी-शद्धि’ द्वारा दूर किया जाए। नाड़ा-शुद्धि में श्वांस क्रिया को यौगिक अनुशासन के द्वारा नियमित किया जाता है।
ज्ञानेन्द्रियों के प्रयोग का अधिकाधिक अभ्यास होना चाहिए। अपर्याप्त प्रयोग से ज्ञानेन्द्रियों की क्षमता का ह्रास होता है। किसी वस्तु को समझने में ज्ञानेन्द्रियों की योग्यता सहायक होती है। निरीक्षण एवं स्मृति में भी ज्ञानेन्द्रियों की क्षमता का प्रभाव पड़ता है, अत: ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में बालकों को रखकर उनकी इन्द्रियों के समुचित प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।
हमारी इन्द्रियाँ ठीक प्रकार से कभी-कभी कार्य नहीं कर पातीं। इसके तीन कारण हैं। स्नायुविक एवं संवेगात्मक प्रवाह पहला कारण है, अतः संवेगों को अनुशासित करना चाहिए और नैतिक आदतों का विकास करना चाहिए। दूसरा कारण मानसिक है जिसके लिए, मानसिक प्रशिक्षण आवश्यक है। तीसरा कारण विगत साहचर्य एवं स्मृति है, जिसके लिए चित्त-शुद्धि एवं चित्त शान्ति आवश्यक है ।
मानसिक प्रशिक्षण (Mental Training)- इन्द्रिय प्रशिक्षण के साथ-साथ मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण पर श्री अरविन्द बल देते हैं। मानस की विकसित अवस्था सूक्ष्म दृष्टि है । मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण में ‘अवधान’ या ध्यान को केन्द्रित करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। ध्यान को केन्द्रित करने में पहले एक वस्तु पर एक समय में ध्यान केन्द्रित करने का अभ्यास किया जा सकता है, किन्तु यही लक्ष्य नहीं है। अवधान को बहुमुखी होना है और कालान्तर में एक समय में अनेक वस्तुओं पर एक साथ ध्यान देने की योग्यता का विकास करना है यह कार्य अभ्यास पर निर्भर है, अतः छात्रों को ध्यान केन्द्रित करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
ध्यान के साथ-साथ बालक की निरीक्षण करने की शक्ति का भी विकास करना है। इसके अतिरिक्त उसकी कण्ठस्थीकरण करने की शक्ति को भी प्रशिक्षित करना है। निरीक्षण, कण्ठस्थीकरण के अतिरिक्त बालक की निर्णायिका शक्ति का भी विकास होना है। मानसिक प्रशिक्षण में कल्पना-शक्ति के विकास पर भी बल देना है। मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण में एक अन्य प्रशिक्षण भी आवश्यक है और वह है बालक की तार्किक शक्तियों का प्रशिक्षण तथ्यों के अनुशीलन द्वारा निष्कर्ष की ट्रेनिंग छात्रों को अवश्य मिलनी चाहिए।
उपर्युक्त सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण के लिए श्री अरविन्द ने ब्रह्मचर्य को महत्त्वपूर्ण माना है। पाश्चात्य भौतिकवादी विचारधारा के अनुसार ब्रह्मचर्य अनावश्यक है। वे सुखवाद के समर्थक हैं किन्तु भारतीय विचारधारा में ब्रह्मचर्य को आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण माना गया है। श्री अरविन्द ही ब्रह्मचर्य के समर्थक हैं। आत्मा एवं सच्चे ज्ञान को अशुद्ध जीवन से नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसके लिए अन्दर और बाहर क पवित्रता आवश्यक है। मस्तिष्क, हृदय, इन्द्रिय एवं विचारों की शुद्धता से व्यक्ति आध्यात्मिक | जगत् में प्रवेश करता है। अतः ब्रह्मचर्य द्वारा सर्वांग शुद्धता का जीवन बिताना आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के समर्थन में श्री अरविन्द अन्य भारतीय आचायों के समान विचार रखते हुए दिखाई पड़ते हैं।
शैक्षिक अभिकरण (Agencies of Education)
विद्यालय-महर्षि अरविन्द विद्यालय को समाज के लघु रूप में देखते थे और विद्यालय का कार्य बालक का भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास करना मानते थे। विद्यालय को बालक का भौतिक विकास करने के लिये श्रेष्ठ भाषाओं, साहित्य, विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिये । उनका विचार था कि मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिये विद्यालयों को मनुष्य में मानवोचित गुणों का विकास करना चाहिये।
परिवार – शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों में श्री अरविन्द के अनुसार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घर है। टैगोर ने बालक के सर्वांगीण विकास हेतु माता की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया हैं।
महर्षि अरविन्द यह मानते हैं कि 7 या 8 वर्ष की अवस्था के पश्चात् बालक की औपचारिक शिक्षा आरम्भ होनी चाहिये। तब तक माता-पिता को ही बालकों को शिक्षा देनी चाहिये।
माताजी का विचार था कि गर्भावस्था में माता को अपने विचार शुद्ध एवं सुन्दर रखने चाहिये। बालक में आशावादी दृष्टिकोण का विकास करना चाहिये। माता-पिता को बच्चों के समक्ष अपने चरित्र एवं व्यवहार द्वारा अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करने चाहिये। माताजी का विचार है कि 12 से 14 वर्ष तक, जब बच्चे सूक्ष्म विचारों को न समझ सकें तब माता-पिता को उपमा, रूपक और दृष्टांत द्वारा सूक्ष्म विचारों को समझाना चाहिये।
राज्य – आज की शिक्षा में राज्य की भूमिका के सम्बन्ध में विवादास्पद विचार हैं। राज्य को शिक्षा में कितना हस्तक्षेप करना चाहिये, इस पर शिक्षाशास्त्री एकमत नहीं हैं। कुछ शिक्षाविद् शिक्षा में राज्य का हस्तक्षेप बिल्कुल पसन्द नहीं करते और कुछ लोग शिक्षा को राज्य के अधीन लाना चाहते हैं।
महर्षि अरविन्द के विचार अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार बिल्कुल स्पष्ट हैं । वह राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार शिक्षा देने के पक्ष में थे। वे राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं, यद्यपि शिक्षा में स्वतन्त्रता के पक्षपाती हैं। महर्षि अरविन्द राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के पक्षपाती थे।
भारतीय संविधान के द्वारा निश्चित किये गये प्रजातांत्रिक मूल्यों को शिक्षा में स्थान दिया गया है तथा आवश्यकतानुसार निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था है। वह राज्य की सहायता से ही सम्भव है।
इस प्रकार श्री अरविन्द ने शिक्षा के अभिकरण के रूप में राज्य की जो भूमिका बतायी है, वर्तमान परिस्थिति में, शिक्षा के क्षेत्र में, राज्य पूर्णरूप से नहीं, परन्तु काफी सीमा तक अपना महत्त्व रखता है।
धार्मिक संस्थायें—महर्षि अरविन्द की शिक्षा में धार्मिक संगठनों का शिक्षा की भूमिका के रूप में किये गये हैं। वे प्रत्येक क्रिया के व्यावहारिक पक्ष पर जोर देते हैं। उनका विचार है कि प्रत्येक धार्मिक संगठन को शुद्ध रूप से सच्चें धर्म की शिक्षा देनी चाहिये । मनुष्य को अन्धविश्वासी की भूल-भूलैयों में नहीं उलझना चाहिये
अरविन्द आश्रम में धार्मिक शिक्षा का विधान रखा गया है और धार्मिक सत्संगों, प्रवचनों द्वारा धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था रहती है परन्तु उस धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में आध्यात्मिक ज्योति को जागृत करना होता है । अतः वे समाज की धार्मिक संस्थाओं एवं अन्य समुदायों को शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु आवश्यक मानते हैं।






